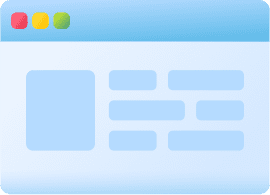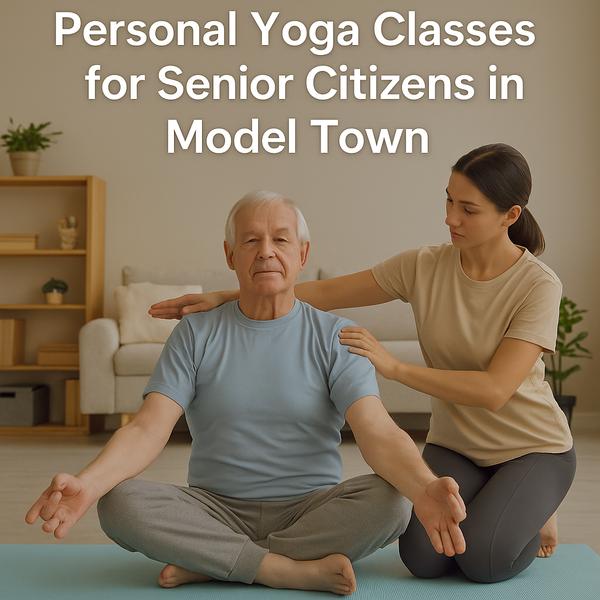
अष्टांग योग (प्रभु मिलन की राह) ...

अष्टांग योग (प्रभु मिलन की राह) पातंजल योग दर्शन में वर्णित महर्षि पतंजलि वर्णित योग सूत्र ही "अष्टांग योग" या राजयोग है। वेदों में वर्णन की हुई योग विद्या का शुद्ध रूप वैदिक काल से लेकर पतंजलि ऋषि के समय तक विशेष रहा। कालांतर में योग के प्रति जनमानस की अरुचि अनुभव करके महर्षि पतंजलि ने स्वयं योग विद्या को सूत्रबद्ध किया। वे ही सूत्र "योग दर्शन" के नाम से प्रसिद्ध है। अष्टांग योग के पालन करने से साधक का मन अत्यंत शांत व एकाग्र चित्त हो जाता है। साधक परम आनंद व संतोष का अनुभव करता है। अष्टांग योग के पालन से साधक अपने आप को परमपिता परमात्मा की छत्रछाया में अनुभव करता है। यमनियमासप्राणायामप्रत्याहारधारणाध्यानसमाधयोष्टा वड़ाग्नि। (योग दर्शन)२९ यम, नियम , आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि योग के आठ अंग "अष्टांग योग" के नाम से प्रसिद्ध हैं। योग के आठ अंगों में प्रथम पांच बहिरंग साधन है और अंतिम तीन अंतरंग साधन है। साधक बहिरंग साधनों की सिद्धि के बिना अंतरंग साधना में सिद्धि प्राप्त नहीं कर सकता। अष्टांग योग में प्रथम यम है।यम उपासना के आधार है। अहिंसासत्यास्तेयब्रह्मचर्यापरिग्रहा यमाः।३० यम 5 हैं। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। 1.(A)अहिंसा- सब प्रकार से सब कालों में प्राणी मात्र को दुख ना देना अहिंसा है। मन से दूसरे को मारना या क्लेश पहुंचाने का विचार करना मानसिक हिंसा है। वाणी से गाली देना या कटु बोलना वाचिक हिंसा है। शरीर से दूसरे प्राणी को दुख देना या मारना शारीरिक हिंसा है। हम जैसा व्यवहार अपने प्रति चाहते हैं वैसे ही व्यवहार हम दूसरों के प्रति करें। साधक को मन, वचन व कर्म से सब के प्रति अहिंसा का भाव रखें पर अपने धर्म और राष्ट्र की रक्षा के लिए अगर शस्त्र उठाना पड़े तो वह हिंसा नहीं है, अपितु वह हमारा कर्तव्य है क्योंकि "वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति" (B). सत्य- जैसा देखा, सुना और जाना जाता है मन , वचन और कर्म से भी वैसे ही व्यवहार करना सत्य कहलाता है। सदाचारी पुरुष जैसा मन में सोचते हैं वैसा ही वाणी से बोलते हैं और जैसा वाणी से बोलते हैं वैसा ही कर्म करते हैं। वेदों में कहा है सत्येनोत्तभिता भूमिः अर्थात सत्य से ही भूमि आदि लोग स्थिर हैं।सत्य का महत्व हम इसी से जान सकते हैं कि परमात्मा के अन्य स्वरूपों में में उसे सत्य स्वरूप भी कहा गया है। (C).अस्तेय- चोरी ना करना, दूसरों के पदार्थ को बिना पूछे प्रयोग करना या उन पर अपना अधिकार जमाना, शास्त्र विरुद्ध ढंग से वस्तुओं का संग्रह करना अस्तेय कहलाता है। बिना परिश्रम के दूसरे के धन को हरना चोरी हैं। अंत है योगी को इस दुष्ट प्रवृत्ति का त्याग कर देना चाहिए। (D).ब्रह्मचर्य- कामवासना को उत्तेजित करने वाले खानपान, दृश्य, श्रव्य, श्रृंगार आदि से सर्वथा बचते हुए वीर्य रक्षा करना ब्रह्मचर्य है। ज्ञानेंद्रियों तथा कर्मेंद्रियों के संयम के लिए उत्तम ग्रंथों का स्वाध्याय करना। निरंतर ओम का जाप करना और ईश्वर का चिंतन करना ब्रह्मचर्य मे परम सहायक हैं। (E).अपरिग्रह - आवश्यकता से अधिक विषयों का सेवन करना, भोग विलास के साधन जो कि साधना में बाधक है एकत्रित करना अपरिग्रह है। साधक को केवल उन वस्तुओं का उपयोग करना चाहिए जो कि उसके साधना में बाधक ना बने। 2.शौचसंतोषतपः स्वाध्यायेश्वरप्रणिधानानि नियमाः। शौच, संतोष, तप , स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान ये पांच नियम है। (A).शौच- शौच का अर्थ है आंतरिक और बाह्य पवित्रता। आंतरिक शुद्धि धर्म आचरण, सत्य भाषण, विद्या, अभ्यास, सत्संग आदि शुभ गुणों के आचरण से होती है और बाहरी शरीर की पवित्रता जल से स्नान करने से, षट्कर्म करने से, प्राणायाम करने से आदि से होती है।साधना करने वाले साधक का मन, तन पवित्र होना चाहिए। (B).संतोष- परिश्रम करने के उपरांत मिले अन्न-धन, विद्या, पद को पाकर उसमें संतोष करना, अर्थात जो आपने सच्चा परिश्रम किया और उसका आपको सत्य फल मिला उसमें संतोष करना। पर संतोष करने का अभिप्राय यह नहीं है कि जो मिला उसके बाद हाथ पर हाथ धरकर बैठ गए अर्थात जो आपके पास है उसमें संतोष करना पर उससे अधिक प्राप्ति के लिए परिश्रम करना ही सच्चा संतोष है। (C).तप- तप का अर्थ है द्वंद्व का सहन करना अर्थात कष्टों को सहन करना। विषम परिस्थितियों में भी अपने लक्ष्य को नहीं छोड़ना। भूख- प्यास, गर्मी -सर्दी, लाभ -हानि , मान -अपमान, जय- पराजय, सुख- दुख आदि कष्टों को समभाव से सहन करना। तप शारीरिक , मानसिक और बौद्धिक तीनों रूपों में किया जाता है। तप के बिना योग में प्रवेश नहीं मिलता तथा सिद्धि प्राप्त नहीं होती। अंतः साधक को तप का अनुष्ठान परम आवश्यक है। (D).स्वाध्याय- आत्मचिंतन करना वैदिक ग्रंथों का अध्ययन करना, आत्मा- परमात्मा विषयों का सूक्ष्म चिंतन करना स्वाध्याय है। परमपिता परमात्मा कि वेद वाणी का स्वाध्याय करना, ब्राह्मण ग्रंथ, उपनिषद, दर्शन आदि वैदिक ग्रंथ साधना में सहायक है। क्योंकि स्वाध्याय मन का भोजन है, आप जैसा स्वाध्याय करेंगे आपका चिंतन भी वैसा ही होगा। (E).ईश्वर प्रणिधान - अर्थात ऐश्वर्या सत्ता को स्वीकार करना ऐश्वर्या वाणी वेद पर विश्वास करना तथा अपने शुभ कर्मों को निष्काम भाव से परमपिता परमात्मा को अर्पण कर देना अर्थात् उनके फल की इच्छा ना करना ईश्वर प्राणी धान है। योग के अंतिम अंग समाधि की प्राप्ति के लिए ईश्वर प्रणी धान सर्वोत्तम साधन है। 3. आसन- स्थिरसुखमासनम् अर्थात ऐसे आसन जिसमें शरीर लंबे समय तक बिना कष्ट के स्थिर रह सके वे आसन यह है जैसे पद्मासन, भद्रासन, स्वस्तिका आसन, दंडासन, सोपाश्रय आसान आदि। यह सब आसन शरीर को सुख देने वाले हैं अर्थात जिस में सुख पूर्वक शरीर और आत्मा स्थिर हो उसको आसन कहते हैं। 4. प्राणायाम- तसि्मन्सति श्वासप्रश्वासयोर्गतिविच्छेदः प्राणायामः। योग दर्शन के अनुसार प्राणायाम चार प्रकार के हैं। वह चार प्राणायाम इस प्रकार से होते हैं कि जब भीतर से बाहर श्वास निकले तब उसको बाहर ही रोक देना इसे प्रथम प्राणायाम कहते हैं। जब बाहर से श्वास अंदर आए तब यथासंभव उसको अंदर ही रोकना यह दूसरा प्राणायाम है ।तीसरा प्राणायाम स्तंभ वृति है कि न तो श्वास को बाहर निकालें नहीं बाहर से भीतर ले जाएं किंतु जितनी देर सुख से रोक सकें उसको जहां का तहां एकदम रोक दें। चौथा प्राणायाम यह है कि जब श्वास अंदर से बाहर को आए तब बाहर ही श्वास को थोड़ा-थोड़ा रोकता रहे और जब श्वास बाहर से अंदर आए तब उसको भी थोड़ा थोड़ा अंदर रोकता रहे इसको बाह्य अभ्यांतर क्षेपी प्राणायाम कहते हैं( प्राणायाम के बारे में विस्तार से अगले लेख में बताएंगे)। 5. प्रत्याहार - प्रत्याहार शब्द का अर्थ है विषयों से विमुख होना। इसमें इंद्रिया बाहरी विषयों से विमुख होकर अंतर्मुखी हो जाती हैं। जब हमारी इंद्रियां अंतर्मुखी हो जाती है तो हम देखते हुए भी नहीं देखते, हमारे कान सुनते हुए भी नहीं सुनते अर्थात् हमारी इंद्रियां विषयों से विमुख हो जाती हैं और हमारा मन हमारा चित्त ध्यान में लगने लगता है यही स्थिति प्रत्याहार है। 6. धारणा - जब उपासना योग के पहले पांच अंग सिद्ध हो जाते हैं तब छटा अंग धारणा भी यथावत प्राप्त होती है। धारणा उसको कहते हैं जब मन को चंचलता से छुड़ाकर नाभि, हृदय , मस्तक, नासिका, जीभ के अग्र भाग आदि स्थान में स्थिर करके ओम का जाप करना धारणा है। 7. ध्यान - महर्षि दयानंद सरस्वती ने ध्यान का प्रकार इस प्रकार बताया है कि धारणा के पीछे उसे स्थान में ध्यान करनेऔर आश्रय लेने के योग्य जो अंतर्यामी व्यापक परमेश्वर है उसके प्रकाश और आनंद में अत्यंत विचार और प्रेम भक्ति के साथ इस प्रकार प्रवेश करना जैसे कि समुंदर में नदी प्रवेश करती है। उस समय ईश्वर को छोड़कर किसी अन्य पदार्थ का समरण नहीं करना अर्थात ईश्वर के स्वरूप में मगन हो जाना ध्यान है। 8. समाधि- महर्षि पतंजलि ने समाधि के विषय में कहा है कि अपने ध्यानात्मक स्वरूप से रहित केवल ध्येय रूप प्रतीत होने वाला ध्यान का नाम समाधि है। समाधि भी दो प्रकार की है संप्रज्ञात समाधि और असंप्रज्ञात समाधि।
Subscribe for latest offers & updates
We hate spam too.